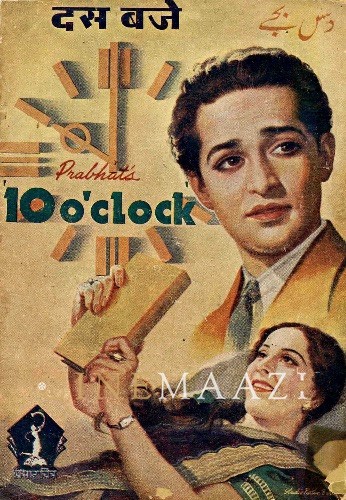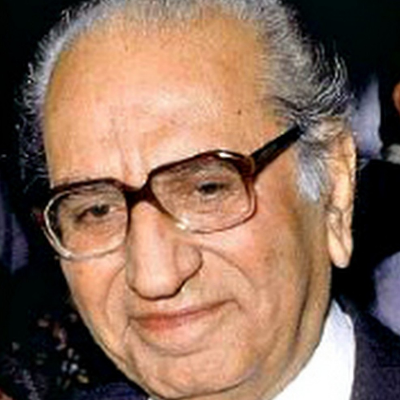हिन्दी फिल्मों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन?
06 Aug, 2022 | Archival Reproductions by Cinemaazi
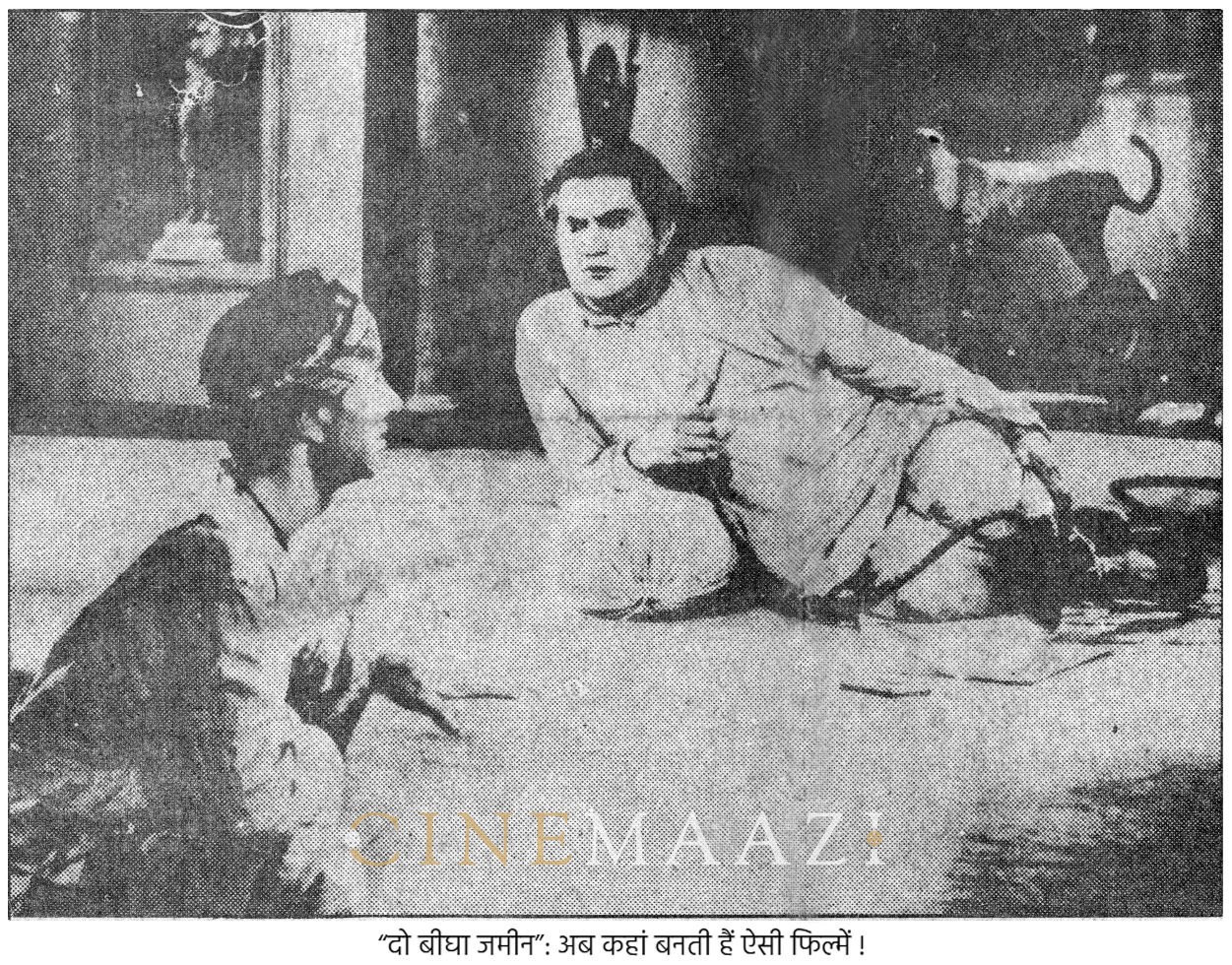
An image from the original article.
Subscribe to read full article
This section is for paid subscribers only. Our subscription is only $37/- for one full year.
You get unlimited access to all paid section and features on the website with this subscription.
Not ready for a full subscription?
You can access this article for $2, and have it saved to your account for one year.
क्या भारतीय सिनेमा - खासकर हिन्दी सिनेमा इतना लम्बा वक्त गुजार आने के बाद भी परिपक्व हो पाया?
पचहत्तर साल हो गए भारतीय फिल्मों को बनते हुए। परिपक्व होने के लिए इतनी उम्र किसी भी सूरत में नाकाफी नहीं कही जा सकती। पर क्या भारतीय सिनेमा - खासकर हिन्दी सिनेमा इतना लम्बा वक्त गुजार आने के बाद भी परिपक्व हो पाया?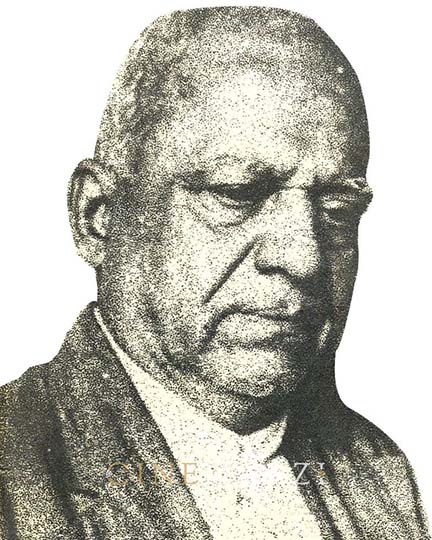
पिछले कुछ वर्षों से जैसी फिल्में बन रही है उन्हें देख कर तो बरबस कहना पड़ता है कि हिन्दी सिनेमा ’परिपक्व’ होने की जगह अपने ’बालपन’ की ओर लौट चला है। जिस हिन्दी सिनेमा ने ’दुनिया न माने’, ’दो बीघा जमीन’, ’आवारा’, ’श्री 420’, ’बंदिनी’, ’सुजाता’, ’मदर इंडिया’, और ’मुगले आजम’ जैसी खूबसूरत फिल्में दीं वहीं आज ’जिस्म का रिश्ता ’ जैसी फूहड़ और अश्लील फिल्में बन रही है। क्या इसी दिन के लिए 75 साल पहले घोर आर्थिक संकटों और सामाजिक उपहासों को सहते हुए दादा फाल्के ने भारतीय फिल्म उद्योग की नींब रखी थी?
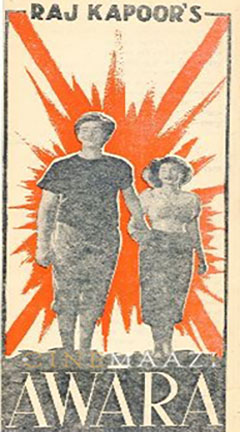
हिन्दी सिनेमा के इस पतन का आखिर जिम्मेदार कौन है निर्माता या दर्शक या फिर दोनों? यह एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर यदि आज विचार करके उसका हल न खोजा गया तो आने वाले दिनों में निश्चय ही बहुत ही दुखद और शर्मनाक परिणाम भोगने पड़ सकते हैं?
हिन्दी सिनेमा के इस पतन का आखिर जिम्मेदार कौन है निर्माता या दर्शक या फिर दोनों? यह एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर यदि आज विचार करके उसका हल न खोजा गया तो आने वाले दिनों में निश्चय ही बहुत ही दुखद और शर्मनाक परिणाम भोगने पड़ सकते हैं?
इस बात पर तो कतई संदेह नहीं किया जा सकता कि बीसवीं सदी में कला के जिस रूप ने भारतीय जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया है- वह सिनेमा है। फिल्में जिस युग में गुंगी थी उस युग (1913-1930) में भी ई. बिलीमोरिया और डी. बिलीमोरिया के जांबाज कारनामों और सुलोचना व गौहर के रूप माधुर्य की सिर्फ एक झलक देखने के लिए लोग सिनेमा हालों की तरफ खिंचे चले आते थे।
उसके बाद सन् 1931 में ’आलम आरा’ के प्रदर्शन के साथ शुभारम्भ हुआ, सवाल फिल्मों के उस खुशनुमा दौर का, जिसने मनोरंजन के क्षेत्र में एक क्रांति सी ला दी। 1931 से 1970 के बीच हिमांशु राय, देवकी बोस, वी. शांताराम, सोहराब मोदी, विजय भट्ट, केदार शर्मा, महबूब, गुरुदत्त, के. आसिफ, चेतन आनंद, राज कपूर और हृषिदा आदि ने जिस तरह मधुर संगीत, उत्कृष्ट अभिनय और दिलों को छू लेने वाली कहानियों से सजी एक से एक खूबसूरत और मर्मस्पर्शी फिल्में देकर हिन्दी सिनेमा का मान बढ़ाया वह किसी से छिपा नहीं है।
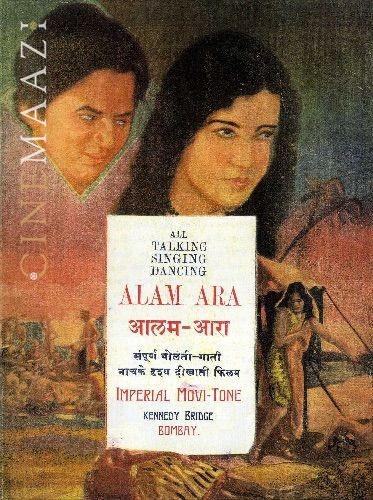
इस दौर में सिनेमा और दर्शक के बीच जो अटूट रिश्ता कायम हुआ, उस रिश्ते को 1970 के बाद हिन्दी फिल्मों के स्तर में आई गिरावट व घरेलू सिनेमा के रूप से उभरे टी.वी. वीडियो जैसे माध्यम भी तोड़ नहीं पाए। आज भी दर्शक उसी शिद्दत और अभिलाषा के साथ सिनेमाहाल पहुंचता है और ब्लैक में टिकट खरीदकर फिल्में देखते हैं। यह बात अलग है कि आज की फिल्में उसे वह आत्मिक संतुष्टि नहीं दे पाती जो 1970 के दौर के पहले की फिल्में देती थी।
यह निःसंदेह स्वीकारना होगा कि आज हिन्दी सिनेमा बल्कि सम्पूर्ण भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो गया है। पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और भव्य सेट देखने को मिल रहे हैं। किन्तु इस तकनीकी समृद्धता और सेटों की भव्यता के फेर में फिल्म निमार्ण की कला जितनी महंगी हो गई उसने फिल्म निर्माताओं का नजरिया ही बदल दिया। अब वह फिल्में समाज की दुखी रगों पर हाथ फेरने, जनमानस के भीतर चेतना लाने या फिल्म कला को समादृत कराने के लिए फिल्में नहीं बनाता बल्कि उसका नजरिया विशुद्ध व्यावसायिक हो गया है।
फिल्म निर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के दामों में आई बेतहाशा वृद्धि और अभिनेता-अभिनेत्रियों के लाखों रुपए का पारिश्रमिकों ने भी बहुत से पुराने निर्माताओं को इस क्षेत्र से अलग हो जाने के लिए विवश कर दिया और उनकी जगह फिल्म कला से सर्वधा अनभिज्ञ जिन विशुद्ध व्यावसायिक घुसपैठियों ने ली उसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। जितनी लागत में पहले पूरी एक फिल्म हो जाती थी- उतना रुपया आज फिल्म के दो-चार झन्नाटेदार सेटों और हीरो-हीरोइन के कपड़ों पर खर्च कर दी जाती है।
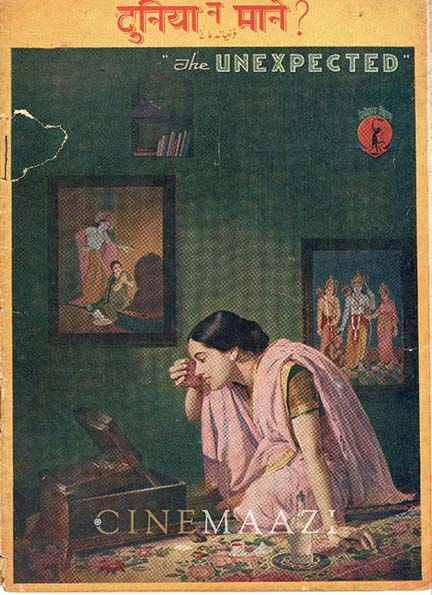
फिल्म निर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के दामों में आई बेतहाशा वृद्धि और अभिनेता-अभिनेत्रियों के लाखों रुपए का पारिश्रमिकों ने भी बहुत से पुराने निर्माताओं को इस क्षेत्र से अलग हो जाने के लिए विवश कर दिया और उनकी जगह फिल्म कला से सर्वधा अनभिज्ञ जिन विशुद्ध व्यावसायिक घुसपैठियों ने ली उसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। जितनी लागत में पहले पूरी एक फिल्म हो जाती थी- उतना रुपया आज फिल्म के दो-चार झन्नाटेदार सेटों और हीरो-हीरोइन के कपड़ों पर खर्च कर दी जाती है।
पहले कहानी लिखे जाने के बाद कहानी के पात्रों पर सटीक बैठने वाले अभिनेता-अभिनेत्रियों का चयन होता था आज पहले अभिनेता-अभिनेत्रियों का चयन होता है और उसके बाद उनके इर्द-गिर्द कहानी का वही घिसापिटा सेक्स व हिंसा से सराबोर तानाबाना बुन लिया जाता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि अभिनेता-अभिनेत्रियों का चयन भी निर्माता फिल्म कला से दूर-दूर तक का वास्ता न रखने वाले फाइनेन्सरों की मर्जी मुताबिक किया करते है और बात यहीं खत्म नहीं हो जाती बल्कि बाद में कहानी (?) और संवादों में फेरबदल प्रमुख अभिनेता व अभिनेत्रियों की मर्जी से होता रहता है। इन हालातों में क्या फिल्म बनेगी इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।
ताज्जुब की बात तो यह है कि अभिनेता-अभिनेत्रियों का चयन भी निर्माता फिल्म कला से दूर-दूर तक का वास्ता न रखने वाले फाइनेन्सरों की मर्जी मुताबिक किया करते है और बात यहीं खत्म नहीं हो जाती बल्कि बाद में कहानी (?) और संवादों में फेरबदल प्रमुख अभिनेता व अभिनेत्रियों की मर्जी से होता रहता है। इन हालातों में क्या फिल्म बनेगी इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।
अब इस पर निर्माताओं का यह कहना कि जो दर्शक चाहते हैं हम वही बनाते हैं - कितना बकवास और हास्यास्पद कथन है उसे सिनेमा की थोड़ी सी मसझ रखने वाला दर्शक भी सहज अनुभव कर सकता है। आज आदमी पहले से कहीं ज्यादा कुंठाग्रस्त और अभिशप्त है वह एक ऐसे अजीब चौराहे पर खड़ा है जहां उसे एक ओर बढ़ती महंगाई, अर्थिक तंगी, अपेक्षा से कम हासिल ओहदे पैसे और व्यवस्था के खिलाफ व्यक्त-अव्यक्त विद्रोह घेरे खड़ा है तो दूसरी तरफ समाज में ऊंचे आसन पर विराजमान लोगों के सजे संवरे शरीर, उनकी मोटरगाड़ियां, आलीशान बंगले और एसो आराम की जिंदगी को देखकर उपजी कुंठा और उस सुख को भोगने का आतुर मन है। ऐसे में व्यक्ति यथार्थ की कडुवाहट से दूर भागकर कल्पना के लोक में खो जाना चाहता है, चाहे यह कुछ घंटों के लिए ही क्यों न हो। सिनेमाहाल के उस अंधेरे माहोल में वह अपने जीवन की सारी उदास हक़ीकतें भूल जाता है। वह गरीबी और व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते अमिताभ बच्चन में अपना प्रति रूप देखना शुरू कर देता है और तब वह अपने भीतर अमिताभ को जीते हुए उसके सात खून को भी माफ कर देता है उसकी रंगीन मिजाजियों में अपने जवान दिलों की धड़कनें सुनता है। यहां उसके सारे भ्रम यथार्थ हो जाते हैं। सच्चे और झूठ के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता और इस दुनिया के बाहर की कोई संस्कृति- राजानीति याद नहीं रहती।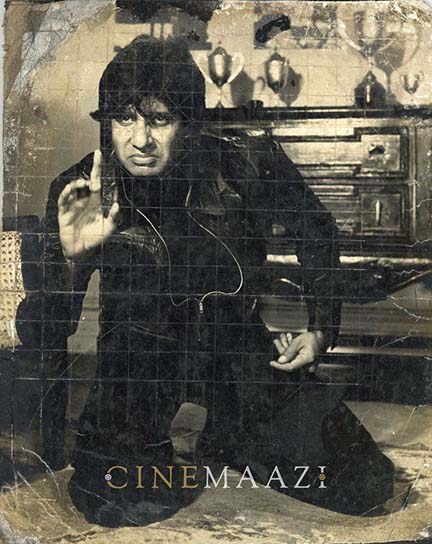
अब यदि आम दर्शक की इस निरीह निस्पृह और निश्छल भावनाओं उसके फिल्म देखने की चाहत को आज की 'ओए ओए...' में चहकती युवा दर्शकों की पसंद का जामा पहनाकर प्रचारित किया जाता है तो सिवाय निर्माताओं और फायनेन्सरों की बुद्धि पर तरस खाने के सिवाय और क्या किया जा सकता है। उनके इसी गलत नजरिए का परिणाम है कि फिल्म कला की जिस आधुनिक समृद्ध तकनीक का उपयोग अच्छी सार्थक फिल्मों में होना चाहिए था वह नहीं हो सका। 1970 के बाद अच्छे अभिनेता अभिनेत्रियों का अकाल पड़ गया था। ऐसी भी बात नहीं।
हिन्दी सिनेमा को संजीव कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, नसिरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अनुपम खेर जैसे अभिनेता और जया भादुड़ी, जरीना वहाब, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी जैसी अभिनेत्रियों की जानदार पीढ़ी मिली थी। जिन्होंने समय-सयम पर मिले कुछेक अवसरों जैसे खामोशी, कोशिश, आनन्द, नमक हराम, अमरप्रेम, दीवार, स्पर्श, आक्रोश, अंकुर, अर्द्ध सत्य, अर्थ और सारांश जैसी फिल्मों में अपने उत्कृष्ट अभिनय क्षमता का प्रमाण दिया पर बाद में पैसे की चमक ने इन सभी को व्यावसायिक सिनेमा की भेड़चाल में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया।
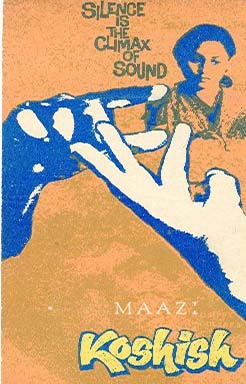
इसी दौर में हिन्दी सिनेमा को संजीव कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, नसिरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अनुपम खेर जैसे अभिनेता और जया भादुड़ी, जरीना वहाब, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी जैसी अभिनेत्रियों की जानदार पीढ़ी मिली थी। जिन्होंने समय-सयम पर मिले कुछेक अवसरों जैसे खामोशी, कोशिश, आनन्द, नमक हराम, अमरप्रेम, दीवार, स्पर्श, आक्रोश, अंकुर, अर्द्ध सत्य, अर्थ और सारांश जैसी फिल्मों में अपने उत्कृष्ट अभिनय क्षमता का प्रमाण दिया पर बाद में पैसे की चमक ने इन सभी को व्यावसायिक सिनेमा की भेड़चाल में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। इस दशक में प्रकाश मेहराओं और मनमोहन देसाइयों जैसे निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार की प्रतिमा का जैसा सर्वोत्कृष्ट दुरुपयोग किया वह हिन्दी सिनेमा में घुस आए इन व्यावसायिक घुसपैठियों और उनकी निकृष्ट सोच को स्वयं उजागर करती है।
अब समय आ गया है कि हिन्दी सिनेमा को एक बार फिर उस ऊंचे सिंहासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए जिस पर वह अब से बीस साल पहले विराजमान था। यह सही है कि वास्तविकता से दूर यानि अयथार्थवादी और आदर्शवादी फिल्मों का अब दौर नहीं रहा। आज तो आम आदमी की जिन्दगी से जुड़ी कहानी उत्कृष्ट अभिनय और मधुर गीत संगीत से सजी फिल्में ही हिन्दी सिनेमा को उसका प्राचीन गौरव वापस दिला सकती है।
This article is from Krishna Kumar Sharma's K K Talkies Series.
Some of the images in the article did not appear with the original article and may not be reproduced without prior permission.
About the Author
Other Articles by Cinemaazi
17 Feb,2024
What is a Good Documentary Film?
25 Jan,2024
Salute to an Immortal Spirit
22 Jan,2024
A Painful Parting
29 Nov,2023
Children's Film Society
28 Oct,2023
Let's Give the Kids a Chance
26 Oct,2023
Directing the Child Actor
25 Oct,2023
Chandu - The Elephant Boy
23 Oct,2023
HEROISM-Children's Film Society gives the lead
18 Oct,2023
Munna
29 Sep,2023
ख्वाजा अहमद अब्बास का पत्र महात्मा गांधी के नाम
02 Sep,2023
Shakti Kapoor: It's Three Punches A Day
04 Jul,2023
Should a Filmmaker be Original?
24 Jun,2023
Babita My First Screen Love
22 Jun,2023
Phir Wohi Dil Laya Hoon
19 Jun,2023
Romance in Our Cinema
12 Jun,2023
The Romance of our Show Houses
12 Jun,2023
Kashmir Ki Kali (1964)
07 Jun,2023
Sangam (1964)
05 Jun,2023
This thing called Love
25 May,2023
Gandhi: Whose voice?
15 May,2023
"Deewar" Becomes a Nation's Prayer
15 May,2023
Mangal Pandey
06 May,2023
History of Cinema, History of the Nation
02 May,2023
Birbal Paristan Mein
20 Apr,2023
Reincarnation... the story goes on ever after
27 Mar,2023
The Film Director?
21 Mar,2023
M Sadiq
15 Mar,2023
The Social Role of the Cinema
15 Mar,2023
"Samaj" A Memorable Film with Popular Appeal
01 Mar,2023
"Two Eyes" in Hollywood
20 Feb,2023
Do Dooni Chaar
15 Feb,2023
Rafoo Chakkar
07 Feb,2023
Johnny Walker.... still going strong
20 Jan,2023
Mahabharat : Epic Tamasha
10 Jan,2023
Narsi Bhagat : An Excellent Biography
03 Jan,2023
Nav Ratri
01 Dec,2022
एक ताजगी का नाम है देवानन्द (Dev Anand)
25 Nov,2022
जे बी एच वाडिया (J B H Wadia) - वचन न जाए
14 Nov,2022
Children's Films in India
01 Sep,2022
Horses .... Cars and Laughs-Mehmood
01 Aug,2022
क्या हिंदी फिल्मों से हास्य गायब हो रहा है?
20 Jul,2022
हास्य की परंपरा और हास्य अभिनेताओं की भूमिका
12 Jul,2022
प्राण और उनकी दाढ़ियाँ
17 Feb,2022
Odds Against a New Comer
10 Dec,2021
Speaking of Portraits and People
03 Nov,2021
An Actor Prepares
19 Oct,2021
Producers' War on Dubbed Films
24 Aug,2021
Jottings from a Film Director's Notebook
26 Jul,2021
प्रेमचंद सत्यजीत राय और ’सद्गति’ -गिरिजाशंकर
22 Jul,2021
Rewind 1990 Commerce of Love Stories
20 Jul,2021
Eastern Scene: Cinema of Surviving Faith
22 Jun,2021
Movie Memories : Tansen (1943)
22 Jun,2021
Movie Memories: Sikandar (1941)
15 Jun,2021
Towards A Brighter Future- Bengali Cinema
20 May,2021
The Enigma Of A Flux - Malayalam Cinema
05 May,2021
The seesaw graph of Hindi filmdom
03 May,2021
Ankahee: The Unspoken
29 Apr,2021
The Mahatma Returns: World Press Reaction
29 Apr,2021
Children’s Films
17 Apr,2021
Telugu Cinema in 1986- Sons and Fathers
09 Apr,2021
Mukhamukham : Face to Face
08 Apr,2021
Tarang : Wages and Profits
01 Apr,2021
Design In Indian Cinema
27 Mar,2021
Movie Memories : Savkari Pash
23 Mar,2021
Double Trouble: Role of Twins In Hindi Cinema
22 Mar,2021
Prem Chopra: The Same Role For Ever
19 Mar,2021
Kalyan Kumar - Karnataka’s Self-Made Star
18 Mar,2021
Ceylon's Cyclonic Cinema
18 Mar,2021
Movie Memories : Aladdin & the Wonderful Lamp
17 Mar,2021
Kumari Padmini: Rising New Star Of The South
11 Mar,2021
50 YEARS OF MALAYALAM CINEMA
02 Mar,2021
Alakh Niranjan: Film India Review
27 Feb,2021
Party: The Story of Choices
26 Feb,2021
The Naushad Era In Hindi Film Music
19 Feb,2021
A Man: Amitabh Bachchan -Amitabh, is My Name
10 Feb,2021
A Man: Amitabh Bachchan - Two of a Kind
29 Jan,2021
Women In Hindi Films : Dichotomy of Values
22 Jan,2021
A Man: Amitabh Bachchan - Yesterday and Tomorrow
22 Jan,2021
Cinema in the South: Crisis of Character
18 Jan,2021
Film Societies Play Their Part
01 Jan,2021
Nutan : A Flashback - The Actress
30 Dec,2020
"Gwalan" Proves A Thrilling Entertainment !
29 Dec,2020
Rajesh Khanna : Echoes Of An Era- Family Of Four
28 Dec,2020
Holi: A Metaphor for Horizontal Violence
23 Dec,2020
A Summon for Mohan Joshi
22 Dec,2020
Nutan : A Flashback - The Friend
22 Dec,2020
Raj Kapoor Scores Personal Triumph In “Aag”!
19 Dec,2020
Smita Patil's Memoir- Trading Places
17 Dec,2020
Shashi Kapoor: Once Upon A Time- The Film Makers
16 Dec,2020
Rajesh Khanna : Echoes Of An Era- Peer Pressures
15 Dec,2020
“Lal Haveli”- Crude But Entertaining!
12 Dec,2020
Nutan : A Flashback - The Wife
10 Dec,2020
Rajesh Khanna : Echoes Of An Era
09 Dec,2020
"Lalkar" Presents Cheap Entertainment
07 Dec,2020
Smita Patil's Memoir-Comrades In Arms
01 Dec,2020
Shashi Kapoor: Once Upon A Time- Unjinxed
28 Nov,2020
Ek Din Ka Sultan- Becomes Good Entertainer !
26 Nov,2020
Smita Patil's Memoir- Friendly Strokes
25 Nov,2020
Shashi Kapoor: Once Upon A Time- Tough Times
07 Nov,2020
The Technician And His Problems
06 Nov,2020
We Must Inject Dynamism Into Publicity
05 Nov,2020
The Role Of Film Finance Corporation
04 Nov,2020
Progress In Raw Film
30 Oct,2020
Freedom In Films
28 Oct,2020
Export Market For Indian Films
23 Oct,2020
The Growth of The Motion Picture
22 Oct,2020
Setup Of The Film Industry
21 Oct,2020
Few Facts About Film Production
13 Oct,2020
Personalisation In Cinema
08 Oct,2020
Waiting for a Doyen's Glance- Arati Bhattacharya
08 Oct,2020
कौन सुनेगा इन सिसकती बिलखती प्रतिभाओं का विलाप?
06 Oct,2020
Asrani - Laugh And The World Laughs With You
05 Oct,2020
My Memorable Roles- Hiralal
03 Oct,2020
राजीव गोस्वामी - कहां थे अब तक 'पेंटर बाबू'?
03 Oct,2020
जब नफरत से बेड़ा पार हो गया: बलराज साहनी
30 Sep,2020
The Case of Emotional Turmoil In Dopatta (1952)
29 Sep,2020
The Story Of A Child Artiste - Sheela Kashimiri
26 Sep,2020
Afsana Likh Rahi Hoon : Tun Tun
26 Sep,2020
Some Hopes For The New Year: Lillian
24 Sep,2020
Joru Ka Bhai: A Tale of 'Atithi Tum Kab Jaoge'
22 Sep,2020
अभिनेता प्रेमअदीब से भेंट
21 Sep,2020
Vijaylaxmi: A Career As The 'Other' Woman
18 Sep,2020
Shaminder: The Actor Who Had High Hopes
16 Sep,2020
धर्मेन्द्र - समय आ रहा है...
14 Sep,2020
Film Life After Fifty : Motilal
14 Sep,2020
प्रसिद्ध फिल्म लेखक गुलशन नंदा से आपकी बातचीत
11 Sep,2020
"I live on hope"- Kumkum
11 Sep,2020
Thehr Zara O Jane Wale : Madhubala Jhaveri
09 Sep,2020
Ratnamala Attracts Attention In ‘Station Master’
08 Sep,2020
Ghory: The Laurel Of Indian Cinema's Comedy Duo
07 Sep,2020
Yeh Teri Saadgi, Yeh Tera Baankpan: Usha Khanna
07 Sep,2020
सेनापति शेट्टी
05 Sep,2020
कृतिदेव यहां मैं, तनूजा, स्वीकार करती हूँ
05 Sep,2020
मै उर्मिला को भूल नहीं पाती - मंजरी
04 Sep,2020
बुलबुल बंगाल की: चंद्राणी मुखर्जी
03 Sep,2020
Payyal's Lucky Break
02 Sep,2020
These Foreign Producers
29 Aug,2020
The Practical Actress: Shabnam
29 Aug,2020
“Amrit” Becomes A First Class Picture
28 Aug,2020
फिल्मी मारपीट के गुरू : अजीम भाई
26 Aug,2020
From Poverty to Screen Fame - Mehboob Khan
26 Aug,2020
Humility: Nasreen's Most Admirable Feature
24 Aug,2020
A Mercenary Comes To India - Bob Christo
23 Aug,2020
Dilip Kumar: The Leader
19 Aug,2020
Alam Ara: Ardeshir Irani's Ambitious Secret
17 Aug,2020
I Serve My Art- Kanan Devi
10 Jul,2020
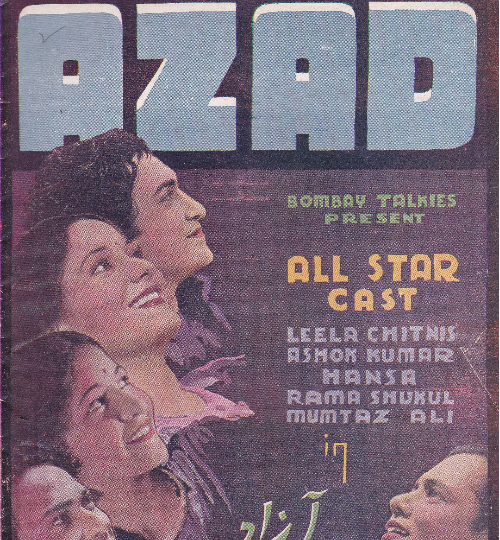

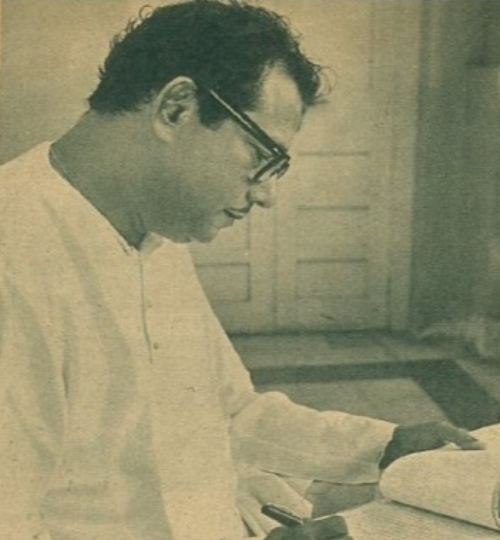

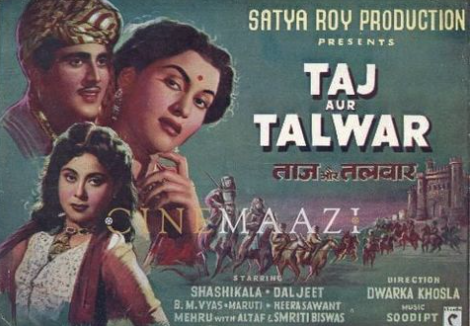

.jpg)