
Image Courtesy: Madhuri, 19 March 1971
'फूल और पत्थर' जैसी फिल्में रोज नहीं बना करती। लेकिन हर कलाकर के जीवन में एक न एक 'फूल और पत्थर' होती जरूर है, जिससे उसे पूरा नाम, यश और ख्याति मिलती है। यह ख्याति ही उस कलाकार को टाइप बना देती है। निर्माता उसके उसी टाइप को बेचते हैं। एक दिन टाइप घिस जाता है कलाकार की फिल्में बाक्स आफिस पर नहीं चलतीं और तब वही निर्मातागण जो उस कलाकार के टाइप को बेचा करते थे, कहने लगते हैं, “एक्टर वेक्टर नहीं चलता जी! कहानी चलती है!”
ताराचंद बड़जात्या कहानी बेचने वाले पहले निर्माता थे। उनकी 'दोस्ती' नये चेहरों के बावजूद भी खूब चली थी। लेकिन ’तकदीर’ में ऐसा कुछ न हो सका। इससे यह तो नहीं हुआ कि उन्होंने कहानी के प्रति आस्था छोड़ दी हो, लेकिन यह उनकी समझ में आ गया कि सही रोल के लिए सही कलाकार का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब उन्होंने 'जीवन मृत्यु’ बनाने की सोची तो उसकी प्रमुख भूमिका के लिए धर्मेन्द्र का नाम सब से आगे था। श्री ताराचंद ने धर्मेन्द्र की फिल्म देखी थी 'फूल और पत्थर’। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हृषिकेश मुखर्जी ने 'फूल और पत्थर’ देखी ही न हो। उन्होंने धर्मेन्द्र की अनेक फिल्में संपादित की थीं। लेकिन उनके साथ संयोग दूसरा था। जब रल्हन धर्मेन्द्र को ले कर ''फूल और पत्थर’ बना रहे थे तब हृषिकेश के साथ धर्मेन्द्र काम कर रहे थे 'अनुपमा’ में। ’अनुपमा’ के दिनों में ही हृषिकेश ने धर्मेन्द्र वचन ले लिया था कि 'सत्यकाम’ में नायक की भूमिका उसे करनी होगी। धर्मेन्द्र ने 'सत्यकाम’ में केवल भूमिका ही स्वीकार नहीं की, हृषिकेश को पंछी जैसा निर्माता भी दिया।
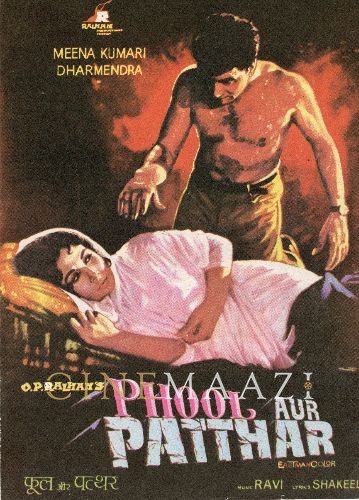
Song booklet cover of Phool Aur Patthar (1966) from Cinemaazi archive
निर्माता-निर्देशक भप्पी सोनी धर्मेन्द्र की फिल्मों से नहीं धर्मेन्द्र से प्रभावित थे। धर्मेन्द्र को वे तब से जानते थे जब उसके पास कोई भूमिका ही नहीं थी। वे फिदा थे तो धर्मेन्द्र के व्यवहार-विचार से। करार आदमी से होना चाहिए, फिल्में तो ससुरी अच्छी-बुरी, हिट-फ्लाप बनती ही रहती है। वे पिछले कई सालों से धर्मेन्द्र से करार करते आ रहे थे और हर साल अपने करार को रिवाइज करा लेते थे। आखिर उनके निर्माता बनने के अवसर भी तभी आया जब 'सत्यकाम’ और 'जीवन मृत्यु’ फ्लोर पर जाने वाली थी। भप्पी ने बड़े प्यार से अपनी फिल्म का नाम रखा, 'तुम हसीं मैं जवां’।
ठीक उन्हीं दिनों प्रोड्यूसर मदन मोहला की स्क्रिप्ट भी रेडी हो गयी। असित सेन ने उस फिल्म का भी निर्देशन किया जिसका नाम 'शराफत’ है। 'शराफत’ न तो धर्मेन्द्र की फिल्म लगती है, न ही असित सेन की। लेकिन वह भी चली। उसके बनने की एक कहानी है।
वादा ऐसा पूरा हुआ
असित सेन की पहली हिंदी फिल्म 'ममता’ में काम करने जब धर्मेन्द्र कलकत्ता पहुंचे थे तो उनपर फिदा हो गये। कलाकार या निर्देशक एक दूसरे पर जब फिदा होता है तो एक ही बात कहता है, ’तुम्हें मेरे साथ एक फिल्म करनी होगी।’ असित सेन ने धर्मेन्द्र से हां कर दी और 'ममता’ के प्रदर्शन के बाद बंबई में थे। एक रात धर्मेन्द्र खुशी-खुशी असित सेन के यहां पहुंचे और उनसे बोले, “मैंने तुम्हारे लिए एक पिक्चर साइन की है।”
“क्या आश्चर्य!” असित सेन ने कहा, “आज ही मैंने तुम्हारे लिए एक पिक्चर साइन की।”
“ठीक है, जब हम दो फिल्मों में एक साथ काम करेंगे।” धमेन्द्र ने कहा।
“तुम अपने प्रोड्यूसर का नाम बताओ।”
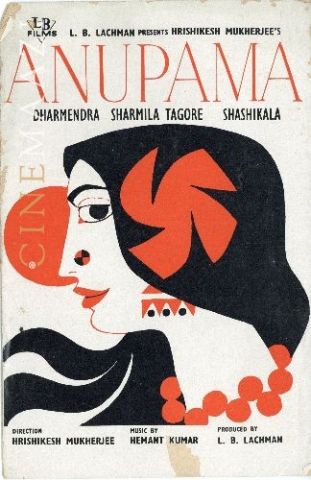
Song booklet cover of Anupama (1966) from Cinemaazi archive
“नहीं, पहले तुम अपने प्रोड्यूसर का नाम बताओ।” फिर दोनों ने जिस प्रोड्यूसर का नाम लिया वह एक ही था, मदन मोहला।
धर्मेन्द्र और असित सेन से अनुबंध कर लेने के बाद मदन मोहला कहानी की तलाश में निकल पड़े। असित सेन को जो कहानियां बेहद पसंद आतीं उन्हें सुन कर मदन का दिल बैठ जाता और जो कहानी उन्हें पसंद आतीं वे मार्किट में आ नहीं रही थी। आखिर बात 'शराफत’ में बनी जिसमें मजमून मदन का था, लिफाफा धर्मेन्द्र का और स्टांप असित सेन का। प्रोड्यूसर को दाद यहां देनी पड़ती है कि उसकी इस फिल्म ने रजत जयंती मनायी।
'सत्यकाम’, 'शराफत’, 'जीवन मृत्यु’ और 'तुम हसीं मैं जवां’ बनाने वाले निर्माता-निर्देशक का धर्मेन्द्र के प्रति अपना-अपना पूर्वाग्रह रहा है। धर्मेन्द्र को उनकी भूमिका देते समय उन्हें इस बात का जैसे अटल विश्वास हो कि उसे सही रोल देने वाले सिर्फ वही एक निर्माता है और बाकियों ने तो उसे समझा ही नहीं। इसके साथ ही उन्हें यह भी लगता रहा कि अगर उनकी भूमिका धर्मेन्द्र ने नहीं की तो दूसरा कौन कर सकेगा?
सचमुच वह रोल धर्मेन्द्र ही कर सकते थे। 'जीवन मृत्यु’ की सफलता के बाद तो यह बात और भी दावे के साथ कही जा सकती है। भारतीय रजतपट पर पहली बार उस फिल्म में एक खूबसूरत सरदार उभरा। विक्रम सिंह ने अपने कौशल और पराक्रम से दुराचारियों को जैसी मात दी वह दर्शकों को चमत्कृत कर गयी। यही तो असली धर्मेन्द्र है, 'फूल और पत्थर’ के बाद।
यह 'इमेज' तोड़ने के लिए...
'फूल और पत्थर’ निर्माताओं और दर्शकों को जितना याद है, धर्मेन्द्र को उतना याद नहीं। धर्मेन्द्र जानता है कि उसका वह इमेज इतना पक्का है कि उसे जब चाहे तब कैश करा सकता है। वह जब भी साका और विक्रम सिंह बन कर परदे पर आयेगा दर्शक तालियां बजायेंगे ही। इसलिए वह ऐसे निर्देशकों को अधिक प्यार करता है जो उसके इस इमेज को तोड़ने में उसकी मदद करते हों। उसके इस रूझान का भी कारण है।
'फूल और पत्थर’ की सफलता के पहले भी धर्मेन्द्र कई बार सफल हो चुका था। 'शोला और शबनम’ उसकी पहली फिल्म थी जिसमें उसने दर्शकों को एक उम्मीद दे दी थी। उस फिल्म में वह किसी को दबाता नहीं दबता है, पीटता नहीं पिटता है। उस फिल्म में वह धरातल पर पैर जमाता है और आकाश को छूता है। उसके बाद उसकी 'बंदिनी’ आयी, एक छोटी साफ़ सुथरी भूमिका। चित्र के प्रारंभ में वह आता है और जल्दी ही परदे से गायब हो जाता है। दर्शक मन में एक कसक ले कर उठते हैं, काश कि वह एक्टर कुछ और पलों के लिए सामने आ जाता। इन्हीं फिल्मों की पंक्ति में उसकी 'बेगाना’ भी आती है। मानसिक अंतद्र्वद्व से पीड़ित एक पति की भूमिका उसने कुशलता से निभायी थी।
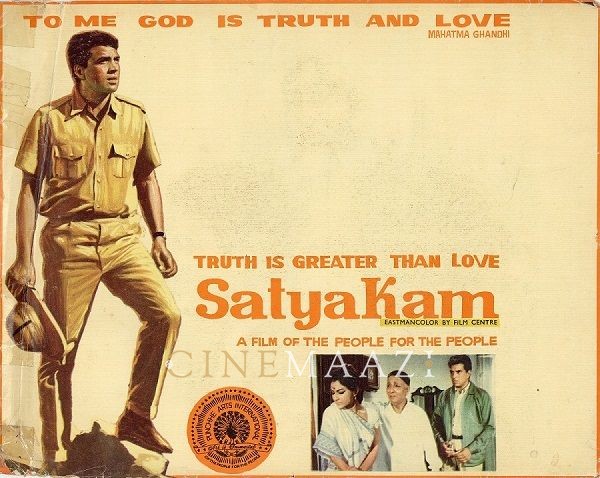
Song booklet cover of Satyakam (1969) from Cinemaazi archive
ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें धर्मेन्द्र कोई गीत नहीं गाये। इस दिशा में शायद वह और भी आगे बढ़ जाता लेकिन तभी कोलंबस को भारत दिख गया। उसकी फिल्म 'फूल और पत्थर’ प्रदर्शित हो गयी। लोग उसे लेकर 'शिकार’, 'आंखें’ और 'जीवन मृत्यु’ का निर्माण करने लगे। धर्मेन्द्र के लिए अच्छी बात सिर्फ यह रही कि इन फिल्मों की सफलता से वह स्वयं विमोहित नहीं हुआ। इन फिल्मों के समानांतर में उसने सप्रयास 'ममता’, 'अनुपमा’, ’शराफत’ और 'सत्यकाम’ को खड़ा रखा है। और इन दो लकीरों के बीच 'तुम हसीं मैं जवां’ तथा 'कब क्यों और कहां’ जैसी फिल्में भी की है।
'सत्यकाम’ सच पूछा जाये तो धर्मेन्द्र के लिए उपासना का विषय रहा। उस भूमिका को उसने कुशलता से निभाया नहीं, हर पल जिया है। चित्र निर्माण के दौरान सत्यप्रिय आचार्य और धर्मेन्द्र दो नहीं रहे थे।
'सत्यकाम’ के प्रदर्शन के बाद लोगों को आश्चर्य हुआ। कथा, अभिनय, निर्देशन की दृष्टि से फिल्म अनूठी थी। जहां लोग सेक्स, अपराध और मारपीट को सफलता का मानदंड बना बैठे हों वहां ऐसी सीधी साधी और सरल फिल्म एक अछूते विषय को ले कर आ जाय तो हैरानी होगी ही।
'सत्यकाम’ जैसी फिल्में भी रोज नहीं बना करतीं। वैसी फिल्मों को कम लोग देखते हैं और अधिक दिनों तक याद रखते हैं। ऐसी फिल्मों में काम करने से श्रेय मिलता है। उस श्रेय का एक मूल्य होता है, जो हर कलाकार को चुकाना पड़ता है। धर्मेन्द्र को भी यह मूल्य चुकाना पड़ा।
लेकिन मुझे खुशी हुई उस दिन जब हृषि दा के साथ राजकीय पुरस्कार लेने वह मद्रास में थे। हृषि दा ने कहा, “धर्मेन्द्र सब कुछ हुआ। लेकिन मुझे अफसोस है तुम्हें मेरी फिल्म की वजह से दुख उठाना पड़ा।” धर्मेन्द्र बोला, “कुछ नहीं दादा, अच्छी फिल्मों का समय आ रहा है न। हम फिर कोशिश करेंगे। एक बार और...”
This is a reproduced article from Madhuri, March 19, 1971 issue.
The images used in the article are from the Cinemaazi archive and were not part of the original article.
ताराचंद बड़जात्या कहानी बेचने वाले पहले निर्माता थे। उनकी 'दोस्ती' नये चेहरों के बावजूद भी खूब चली थी। लेकिन ’तकदीर’ में ऐसा कुछ न हो सका। इससे यह तो नहीं हुआ कि उन्होंने कहानी के प्रति आस्था छोड़ दी हो, लेकिन यह उनकी समझ में आ गया कि सही रोल के लिए सही कलाकार का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब उन्होंने 'जीवन मृत्यु’ बनाने की सोची तो उसकी प्रमुख भूमिका के लिए धर्मेन्द्र का नाम सब से आगे था। श्री ताराचंद ने धर्मेन्द्र की फिल्म देखी थी 'फूल और पत्थर’। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हृषिकेश मुखर्जी ने 'फूल और पत्थर’ देखी ही न हो। उन्होंने धर्मेन्द्र की अनेक फिल्में संपादित की थीं। लेकिन उनके साथ संयोग दूसरा था। जब रल्हन धर्मेन्द्र को ले कर ''फूल और पत्थर’ बना रहे थे तब हृषिकेश के साथ धर्मेन्द्र काम कर रहे थे 'अनुपमा’ में। ’अनुपमा’ के दिनों में ही हृषिकेश ने धर्मेन्द्र वचन ले लिया था कि 'सत्यकाम’ में नायक की भूमिका उसे करनी होगी। धर्मेन्द्र ने 'सत्यकाम’ में केवल भूमिका ही स्वीकार नहीं की, हृषिकेश को पंछी जैसा निर्माता भी दिया।
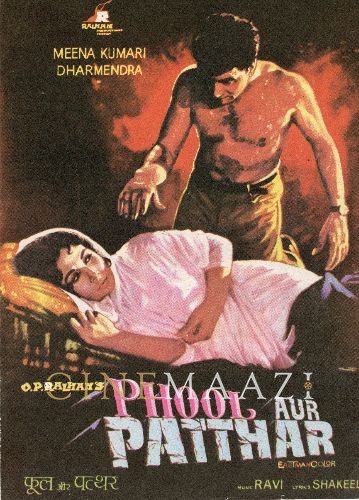
निर्माता-निर्देशक भप्पी सोनी धर्मेन्द्र की फिल्मों से नहीं धर्मेन्द्र से प्रभावित थे। धर्मेन्द्र को वे तब से जानते थे जब उसके पास कोई भूमिका ही नहीं थी। वे फिदा थे तो धर्मेन्द्र के व्यवहार-विचार से। करार आदमी से होना चाहिए, फिल्में तो ससुरी अच्छी-बुरी, हिट-फ्लाप बनती ही रहती है। वे पिछले कई सालों से धर्मेन्द्र से करार करते आ रहे थे और हर साल अपने करार को रिवाइज करा लेते थे। आखिर उनके निर्माता बनने के अवसर भी तभी आया जब 'सत्यकाम’ और 'जीवन मृत्यु’ फ्लोर पर जाने वाली थी। भप्पी ने बड़े प्यार से अपनी फिल्म का नाम रखा, 'तुम हसीं मैं जवां’।
ठीक उन्हीं दिनों प्रोड्यूसर मदन मोहला की स्क्रिप्ट भी रेडी हो गयी। असित सेन ने उस फिल्म का भी निर्देशन किया जिसका नाम 'शराफत’ है। 'शराफत’ न तो धर्मेन्द्र की फिल्म लगती है, न ही असित सेन की। लेकिन वह भी चली। उसके बनने की एक कहानी है।
वादा ऐसा पूरा हुआ
असित सेन की पहली हिंदी फिल्म 'ममता’ में काम करने जब धर्मेन्द्र कलकत्ता पहुंचे थे तो उनपर फिदा हो गये। कलाकार या निर्देशक एक दूसरे पर जब फिदा होता है तो एक ही बात कहता है, ’तुम्हें मेरे साथ एक फिल्म करनी होगी।’ असित सेन ने धर्मेन्द्र से हां कर दी और 'ममता’ के प्रदर्शन के बाद बंबई में थे। एक रात धर्मेन्द्र खुशी-खुशी असित सेन के यहां पहुंचे और उनसे बोले, “मैंने तुम्हारे लिए एक पिक्चर साइन की है।”
“क्या आश्चर्य!” असित सेन ने कहा, “आज ही मैंने तुम्हारे लिए एक पिक्चर साइन की।”
“ठीक है, जब हम दो फिल्मों में एक साथ काम करेंगे।” धमेन्द्र ने कहा।
“तुम अपने प्रोड्यूसर का नाम बताओ।”
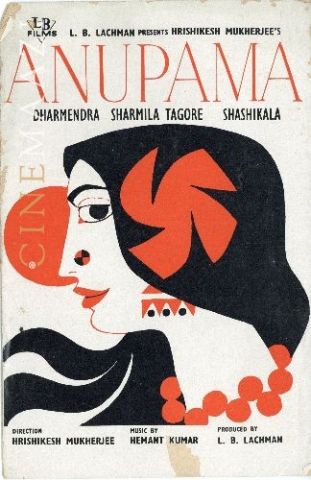
“नहीं, पहले तुम अपने प्रोड्यूसर का नाम बताओ।” फिर दोनों ने जिस प्रोड्यूसर का नाम लिया वह एक ही था, मदन मोहला।
धर्मेन्द्र और असित सेन से अनुबंध कर लेने के बाद मदन मोहला कहानी की तलाश में निकल पड़े। असित सेन को जो कहानियां बेहद पसंद आतीं उन्हें सुन कर मदन का दिल बैठ जाता और जो कहानी उन्हें पसंद आतीं वे मार्किट में आ नहीं रही थी। आखिर बात 'शराफत’ में बनी जिसमें मजमून मदन का था, लिफाफा धर्मेन्द्र का और स्टांप असित सेन का। प्रोड्यूसर को दाद यहां देनी पड़ती है कि उसकी इस फिल्म ने रजत जयंती मनायी।
'सत्यकाम’, 'शराफत’, 'जीवन मृत्यु’ और 'तुम हसीं मैं जवां’ बनाने वाले निर्माता-निर्देशक का धर्मेन्द्र के प्रति अपना-अपना पूर्वाग्रह रहा है। धर्मेन्द्र को उनकी भूमिका देते समय उन्हें इस बात का जैसे अटल विश्वास हो कि उसे सही रोल देने वाले सिर्फ वही एक निर्माता है और बाकियों ने तो उसे समझा ही नहीं। इसके साथ ही उन्हें यह भी लगता रहा कि अगर उनकी भूमिका धर्मेन्द्र ने नहीं की तो दूसरा कौन कर सकेगा?
सचमुच वह रोल धर्मेन्द्र ही कर सकते थे। 'जीवन मृत्यु’ की सफलता के बाद तो यह बात और भी दावे के साथ कही जा सकती है। भारतीय रजतपट पर पहली बार उस फिल्म में एक खूबसूरत सरदार उभरा। विक्रम सिंह ने अपने कौशल और पराक्रम से दुराचारियों को जैसी मात दी वह दर्शकों को चमत्कृत कर गयी। यही तो असली धर्मेन्द्र है, 'फूल और पत्थर’ के बाद।
यह 'इमेज' तोड़ने के लिए...
'फूल और पत्थर’ निर्माताओं और दर्शकों को जितना याद है, धर्मेन्द्र को उतना याद नहीं। धर्मेन्द्र जानता है कि उसका वह इमेज इतना पक्का है कि उसे जब चाहे तब कैश करा सकता है। वह जब भी साका और विक्रम सिंह बन कर परदे पर आयेगा दर्शक तालियां बजायेंगे ही। इसलिए वह ऐसे निर्देशकों को अधिक प्यार करता है जो उसके इस इमेज को तोड़ने में उसकी मदद करते हों। उसके इस रूझान का भी कारण है।
'फूल और पत्थर’ की सफलता के पहले भी धर्मेन्द्र कई बार सफल हो चुका था। 'शोला और शबनम’ उसकी पहली फिल्म थी जिसमें उसने दर्शकों को एक उम्मीद दे दी थी। उस फिल्म में वह किसी को दबाता नहीं दबता है, पीटता नहीं पिटता है। उस फिल्म में वह धरातल पर पैर जमाता है और आकाश को छूता है। उसके बाद उसकी 'बंदिनी’ आयी, एक छोटी साफ़ सुथरी भूमिका। चित्र के प्रारंभ में वह आता है और जल्दी ही परदे से गायब हो जाता है। दर्शक मन में एक कसक ले कर उठते हैं, काश कि वह एक्टर कुछ और पलों के लिए सामने आ जाता। इन्हीं फिल्मों की पंक्ति में उसकी 'बेगाना’ भी आती है। मानसिक अंतद्र्वद्व से पीड़ित एक पति की भूमिका उसने कुशलता से निभायी थी।
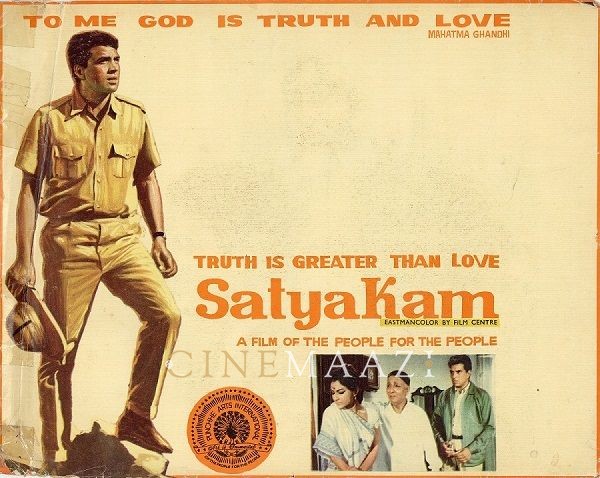
ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें धर्मेन्द्र कोई गीत नहीं गाये। इस दिशा में शायद वह और भी आगे बढ़ जाता लेकिन तभी कोलंबस को भारत दिख गया। उसकी फिल्म 'फूल और पत्थर’ प्रदर्शित हो गयी। लोग उसे लेकर 'शिकार’, 'आंखें’ और 'जीवन मृत्यु’ का निर्माण करने लगे। धर्मेन्द्र के लिए अच्छी बात सिर्फ यह रही कि इन फिल्मों की सफलता से वह स्वयं विमोहित नहीं हुआ। इन फिल्मों के समानांतर में उसने सप्रयास 'ममता’, 'अनुपमा’, ’शराफत’ और 'सत्यकाम’ को खड़ा रखा है। और इन दो लकीरों के बीच 'तुम हसीं मैं जवां’ तथा 'कब क्यों और कहां’ जैसी फिल्में भी की है।
'सत्यकाम’ सच पूछा जाये तो धर्मेन्द्र के लिए उपासना का विषय रहा। उस भूमिका को उसने कुशलता से निभाया नहीं, हर पल जिया है। चित्र निर्माण के दौरान सत्यप्रिय आचार्य और धर्मेन्द्र दो नहीं रहे थे।
'सत्यकाम’ के प्रदर्शन के बाद लोगों को आश्चर्य हुआ। कथा, अभिनय, निर्देशन की दृष्टि से फिल्म अनूठी थी। जहां लोग सेक्स, अपराध और मारपीट को सफलता का मानदंड बना बैठे हों वहां ऐसी सीधी साधी और सरल फिल्म एक अछूते विषय को ले कर आ जाय तो हैरानी होगी ही।
'सत्यकाम’ जैसी फिल्में भी रोज नहीं बना करतीं। वैसी फिल्मों को कम लोग देखते हैं और अधिक दिनों तक याद रखते हैं। ऐसी फिल्मों में काम करने से श्रेय मिलता है। उस श्रेय का एक मूल्य होता है, जो हर कलाकार को चुकाना पड़ता है। धर्मेन्द्र को भी यह मूल्य चुकाना पड़ा।
लेकिन मुझे खुशी हुई उस दिन जब हृषि दा के साथ राजकीय पुरस्कार लेने वह मद्रास में थे। हृषि दा ने कहा, “धर्मेन्द्र सब कुछ हुआ। लेकिन मुझे अफसोस है तुम्हें मेरी फिल्म की वजह से दुख उठाना पड़ा।” धर्मेन्द्र बोला, “कुछ नहीं दादा, अच्छी फिल्मों का समय आ रहा है न। हम फिर कोशिश करेंगे। एक बार और...”
This is a reproduced article from Madhuri, March 19, 1971 issue.
The images used in the article are from the Cinemaazi archive and were not part of the original article.
About the Author
Other Articles by Cinemaazi
17 Feb,2024
What is a Good Documentary Film?
25 Jan,2024
Salute to an Immortal Spirit
22 Jan,2024
A Painful Parting
29 Nov,2023
Children's Film Society
28 Oct,2023
Let's Give the Kids a Chance
26 Oct,2023
Directing the Child Actor
25 Oct,2023
Chandu - The Elephant Boy
23 Oct,2023
HEROISM-Children's Film Society gives the lead
18 Oct,2023
Munna
29 Sep,2023
ख्वाजा अहमद अब्बास का पत्र महात्मा गांधी के नाम
02 Sep,2023
Shakti Kapoor: It's Three Punches A Day
04 Jul,2023
Should a Filmmaker be Original?
24 Jun,2023
Babita My First Screen Love
22 Jun,2023
Phir Wohi Dil Laya Hoon
19 Jun,2023
Romance in Our Cinema
12 Jun,2023
The Romance of our Show Houses
12 Jun,2023
Kashmir Ki Kali (1964)
07 Jun,2023
Sangam (1964)
05 Jun,2023
This thing called Love
25 May,2023
Gandhi: Whose voice?
15 May,2023
"Deewar" Becomes a Nation's Prayer
15 May,2023
Mangal Pandey
06 May,2023
History of Cinema, History of the Nation
02 May,2023
Birbal Paristan Mein
20 Apr,2023
Reincarnation... the story goes on ever after
27 Mar,2023
The Film Director?
21 Mar,2023
M Sadiq
15 Mar,2023
The Social Role of the Cinema
15 Mar,2023
"Samaj" A Memorable Film with Popular Appeal
01 Mar,2023
"Two Eyes" in Hollywood
20 Feb,2023
Do Dooni Chaar
15 Feb,2023
Rafoo Chakkar
07 Feb,2023
Johnny Walker.... still going strong
20 Jan,2023
Mahabharat : Epic Tamasha
10 Jan,2023
Narsi Bhagat : An Excellent Biography
03 Jan,2023
Nav Ratri
01 Dec,2022
एक ताजगी का नाम है देवानन्द (Dev Anand)
25 Nov,2022
जे बी एच वाडिया (J B H Wadia) - वचन न जाए
14 Nov,2022
Children's Films in India
01 Sep,2022
Horses .... Cars and Laughs-Mehmood
06 Aug,2022
हिन्दी फिल्मों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन?
01 Aug,2022
क्या हिंदी फिल्मों से हास्य गायब हो रहा है?
20 Jul,2022
हास्य की परंपरा और हास्य अभिनेताओं की भूमिका
12 Jul,2022
प्राण और उनकी दाढ़ियाँ
17 Feb,2022
Odds Against a New Comer
10 Dec,2021
Speaking of Portraits and People
03 Nov,2021
An Actor Prepares
19 Oct,2021
Producers' War on Dubbed Films
24 Aug,2021
Jottings from a Film Director's Notebook
26 Jul,2021
प्रेमचंद सत्यजीत राय और ’सद्गति’ -गिरिजाशंकर
22 Jul,2021
Rewind 1990 Commerce of Love Stories
20 Jul,2021
Eastern Scene: Cinema of Surviving Faith
22 Jun,2021
Movie Memories : Tansen (1943)
22 Jun,2021
Movie Memories: Sikandar (1941)
15 Jun,2021
Towards A Brighter Future- Bengali Cinema
20 May,2021
The Enigma Of A Flux - Malayalam Cinema
05 May,2021
The seesaw graph of Hindi filmdom
03 May,2021
Ankahee: The Unspoken
29 Apr,2021
The Mahatma Returns: World Press Reaction
29 Apr,2021
Children’s Films
17 Apr,2021
Telugu Cinema in 1986- Sons and Fathers
09 Apr,2021
Mukhamukham : Face to Face
08 Apr,2021
Tarang : Wages and Profits
01 Apr,2021
Design In Indian Cinema
27 Mar,2021
Movie Memories : Savkari Pash
23 Mar,2021
Double Trouble: Role of Twins In Hindi Cinema
22 Mar,2021
Prem Chopra: The Same Role For Ever
19 Mar,2021
Kalyan Kumar - Karnataka’s Self-Made Star
18 Mar,2021
Ceylon's Cyclonic Cinema
18 Mar,2021
Movie Memories : Aladdin & the Wonderful Lamp
17 Mar,2021
Kumari Padmini: Rising New Star Of The South
11 Mar,2021
50 YEARS OF MALAYALAM CINEMA
02 Mar,2021
Alakh Niranjan: Film India Review
27 Feb,2021
Party: The Story of Choices
26 Feb,2021
The Naushad Era In Hindi Film Music
19 Feb,2021
A Man: Amitabh Bachchan -Amitabh, is My Name
10 Feb,2021
A Man: Amitabh Bachchan - Two of a Kind
29 Jan,2021
Women In Hindi Films : Dichotomy of Values
22 Jan,2021
A Man: Amitabh Bachchan - Yesterday and Tomorrow
22 Jan,2021
Cinema in the South: Crisis of Character
18 Jan,2021
Film Societies Play Their Part
01 Jan,2021
Nutan : A Flashback - The Actress
30 Dec,2020
"Gwalan" Proves A Thrilling Entertainment !
29 Dec,2020
Rajesh Khanna : Echoes Of An Era- Family Of Four
28 Dec,2020
Holi: A Metaphor for Horizontal Violence
23 Dec,2020
A Summon for Mohan Joshi
22 Dec,2020
Nutan : A Flashback - The Friend
22 Dec,2020
Raj Kapoor Scores Personal Triumph In “Aag”!
19 Dec,2020
Smita Patil's Memoir- Trading Places
17 Dec,2020
Shashi Kapoor: Once Upon A Time- The Film Makers
16 Dec,2020
Rajesh Khanna : Echoes Of An Era- Peer Pressures
15 Dec,2020
“Lal Haveli”- Crude But Entertaining!
12 Dec,2020
Nutan : A Flashback - The Wife
10 Dec,2020
Rajesh Khanna : Echoes Of An Era
09 Dec,2020
"Lalkar" Presents Cheap Entertainment
07 Dec,2020
Smita Patil's Memoir-Comrades In Arms
01 Dec,2020
Shashi Kapoor: Once Upon A Time- Unjinxed
28 Nov,2020
Ek Din Ka Sultan- Becomes Good Entertainer !
26 Nov,2020
Smita Patil's Memoir- Friendly Strokes
25 Nov,2020
Shashi Kapoor: Once Upon A Time- Tough Times
07 Nov,2020
The Technician And His Problems
06 Nov,2020
We Must Inject Dynamism Into Publicity
05 Nov,2020
The Role Of Film Finance Corporation
04 Nov,2020
Progress In Raw Film
30 Oct,2020
Freedom In Films
28 Oct,2020
Export Market For Indian Films
23 Oct,2020
The Growth of The Motion Picture
22 Oct,2020
Setup Of The Film Industry
21 Oct,2020
Few Facts About Film Production
13 Oct,2020
Personalisation In Cinema
08 Oct,2020
Waiting for a Doyen's Glance- Arati Bhattacharya
08 Oct,2020
कौन सुनेगा इन सिसकती बिलखती प्रतिभाओं का विलाप?
06 Oct,2020
Asrani - Laugh And The World Laughs With You
05 Oct,2020
My Memorable Roles- Hiralal
03 Oct,2020
राजीव गोस्वामी - कहां थे अब तक 'पेंटर बाबू'?
03 Oct,2020
जब नफरत से बेड़ा पार हो गया: बलराज साहनी
30 Sep,2020
The Case of Emotional Turmoil In Dopatta (1952)
29 Sep,2020
The Story Of A Child Artiste - Sheela Kashimiri
26 Sep,2020
Afsana Likh Rahi Hoon : Tun Tun
26 Sep,2020
Some Hopes For The New Year: Lillian
24 Sep,2020
Joru Ka Bhai: A Tale of 'Atithi Tum Kab Jaoge'
22 Sep,2020
अभिनेता प्रेमअदीब से भेंट
21 Sep,2020
Vijaylaxmi: A Career As The 'Other' Woman
18 Sep,2020
Shaminder: The Actor Who Had High Hopes
14 Sep,2020
Film Life After Fifty : Motilal
14 Sep,2020
प्रसिद्ध फिल्म लेखक गुलशन नंदा से आपकी बातचीत
11 Sep,2020
"I live on hope"- Kumkum
11 Sep,2020
Thehr Zara O Jane Wale : Madhubala Jhaveri
09 Sep,2020
Ratnamala Attracts Attention In ‘Station Master’
08 Sep,2020
Ghory: The Laurel Of Indian Cinema's Comedy Duo
07 Sep,2020
Yeh Teri Saadgi, Yeh Tera Baankpan: Usha Khanna
07 Sep,2020
सेनापति शेट्टी
05 Sep,2020
कृतिदेव यहां मैं, तनूजा, स्वीकार करती हूँ
05 Sep,2020
मै उर्मिला को भूल नहीं पाती - मंजरी
04 Sep,2020
बुलबुल बंगाल की: चंद्राणी मुखर्जी
03 Sep,2020
Payyal's Lucky Break
02 Sep,2020
These Foreign Producers
29 Aug,2020
The Practical Actress: Shabnam
29 Aug,2020
“Amrit” Becomes A First Class Picture
28 Aug,2020
फिल्मी मारपीट के गुरू : अजीम भाई
26 Aug,2020
From Poverty to Screen Fame - Mehboob Khan
26 Aug,2020
Humility: Nasreen's Most Admirable Feature
24 Aug,2020
A Mercenary Comes To India - Bob Christo
23 Aug,2020
Dilip Kumar: The Leader
19 Aug,2020
Alam Ara: Ardeshir Irani's Ambitious Secret
17 Aug,2020
I Serve My Art- Kanan Devi
10 Jul,2020






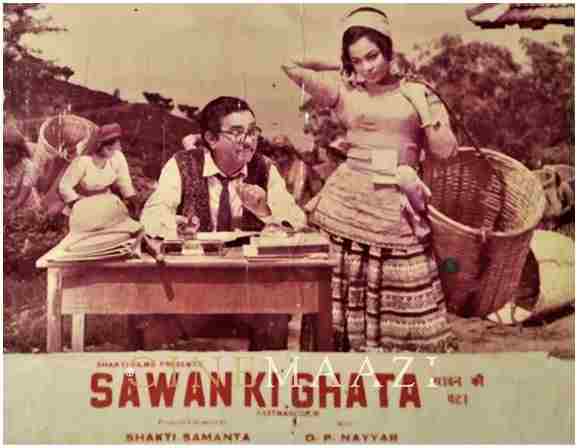
.jpg)


